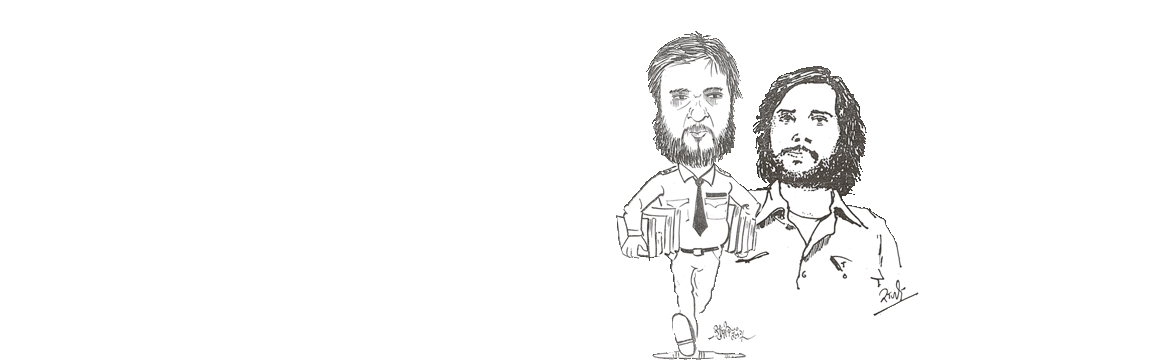![]()
यह अश्वमेध यज्ञ का नहीं, राजसूय यज्ञ का समय है। यह बहेलियों के जाल को तार-तार करने का वक़्त है। ‘नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने । विक्रमार्जितसत्त्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता ।।’ शेर को जंगल का राजा नियुक्त करने के लिए न तो कोई राज्याभिषेक किया जाता है और न कोई पूजा-पाठी संस्कार। राहुल मुझ नाचीज़ की सुनें तो ठीक, न सुनें तो ठीक। अपनी बात कहना अपना काम है।
कल राजीव गांधी का जन्म दिन था और अगर त्रासद हादसे ने उन्हें न छीना होता तो आज वे ज़रूर हमारे साथ होते और 77 बरस के होते। आजकल 77 की उम्र होती ही क्या है? मोतीलाल वोरा शरीर से भले ही थोड़े थक गए थे, मगर दिमाग़ी तौर पर 92 की उम्र तक चुस्त रहे और कांग्रेस मुख्यालय में नियमित बैठ कर काम करते रहे। लालकृष्ण आडवाणी 93 के हैं और हर लिहाज़ से चुस्त-दुरुस्त हैं। डॉ. कर्ण सिंह 90 के हैं और कई नौजवानों से बेहतर सेहत है उनकी। मुरली मनोहर जोशी 87 के हैं और खूब स्वस्थ हैं। शिवराज पाटिल 85 के हैं और वैसे-के-वैसे हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे 79 के हैं और रोज़ ताल ठोकते हैं।
लोकसभा के मौजूदा सदस्य शफ़ीकुर्रहमान बर्क 91 के हैं। फ़ारूक अब्दुल्ला और चौधरी मोहन जटुआ 83 के हैं। मुहम्मद सादिक 82 के हैं। मुलायम सिंह यादव 81 के हैं। टी. आर. बालू, अबू हसीम खान चौधरी, श्रीनिवास दादासाहब पाटिल और सिद्दप्पा बसवराज 80 के हैं। राज्यसभा में दोनों पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और एच.डी. देवेगौड़ा 88 साल के हैं। सुखदेव सिंह ढींडसा 85 के हैं। के. केशवराव और एस.आर. बालासुब्रह्मण्यम 82 के हैं। सुब्रह्मण्यन स्वामी, महेंद्र प्रसाद, एम. षण्मुगम और लक्ष्मीकांत राव 81 के हैं। शरद पवार, ऑस्कर फर्नांडिस और हरनाथ सिंह यादव 80 के हैं।
तो राजीव गांधी तो आज की लोकसभा में 79 के शिशिर अधिकारी और राज्यसभा में 78 साल की अंबिका सोनी से भी छोटे होते। सोचिए कि अगर वे होते तो आज की संसद कैसी होती? अंदाज़ लगाइए कि अगर वे होते तो आज की कांग्रेस कैसी होती? अगर वे होते तो आज की भारतीय जनता पार्टी कैसी होती? वे होते तो क्या नरेंद्र भाई मोदी आज अपने को हिंदुओं का हृदय-सम्राट घोषित कर प्रधानमंत्री बने बैठे होते? अगर राजीव गांधी आज होते तो देश की अर्थव्यवस्था ऐसी बदहाल होती? अगर वे होते तो किसी भी महामारी के वक़्त क्या मोर से खेल रहे होते? वे होते तो क्या राजनय के संसार में भारत की ऐसी फ़ज़ीहत हो रही होती?
राजीव गांधी होते तो वे पामुलपर्ति वेंकट नरसिंहराव प्रधानमंत्री नहीं होते, जिनके राज में भारत का सामाजिक जीवन दो-फाड़ होने पर बाक़ायदा मुहर लगी। जिनके राज में देश के आर्थिक-भाखड़ा के सारे दरवाज़े ऐसे खुले कि भरभरा कर आई उदारीकरण की बाढ़ में बहुत कुछ बह कर इधर-उधर चला गया। राजीव होते तो अटल बिहारी वाजपेयी भी शायद प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। वाजपेयी भले ही बहुत भले थे, लेकिन उनके जमाने में ही सरकारी अंगने में आमोद-प्रमोद और रंजन-मनोरंजन को संस्थागत स्वरूप मिला। अटल जी के आंख-कान-नाक प्रमोद महाजन और दत्तक दामाद रंजन भट्टाचार्य के बोए बीजों ने राजनीति और कारोबार की दुनिया को ऐसी सतरंगी फ़सल से नवाज़ा कि क्या कहूं?
राजीव गांधी होते तो देश का साबका हरदनहल्ली देवेगौड़ा और इंदर कुमार गुजराल से भी नहीं पड़ता। सत्ता के दलालों की प्रधानमंत्री कार्यालय में जैसी आवभगत देवेगौड़ा के वक़्त में हुई, भूतो न भविष्यति थी। विजय माल्या को भूमिपुत्र मानने वाले देवेगौड़ा ने उनके लिए दो बार राज्यसभा का दरवाज़ा खोला था। उनके सियासी नृत्यांगन का परदा इतना झीना था कि ऐसों-ऐसों ने ताकझांक कर ली, जो कभी अपने घर से बाहर भी नहीं निकले थे। इंदर कुमार गुजराल ने तो प्रधानमंत्री बन कर वह किया कि कोई मूढ़ भी न करता। उनके ‘गुजराल-सिद्धांत’ का नतीजा देश को बहुत भुगतना पड़ा। प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजराल ने रॉ की पाकिस्तान-डेस्क को ही पोटली में बांध कर रख दिया। करगिल इसी निर्णय की देन था। नेपाल का कालापानी विवाद भी गुजराल के सौजन्य से ही भारत के गले पड़ा। 1997 की गर्मियों में जब वे नेपाल गए तो वहां की सरकार ने पहली बार बाकायदा यह मसला उनके सामने उठाया और प्रतिकार करने के बजाय गुजराल सिले होंठ लिए लौट आए।
इसलिए जिन्हें आज लग रहा है कि 56 इंच के किसी सीने से चिपक कर उनका जीवन धन्य हो गया है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर महज़ 46 साल की उम्र में राजीव गांधी को विश्व-शक्तियों ने अपने रास्ते से न हटाया होता तो भारत आज उस रास्ते पर चल रहा होता कि दुनिया उसके पीछे होती। हम विश्व-गुरु बनने के थोथे दावे नहीं कर होते। हम सचमुच विश्व-गुरु होते। इसलिए कि राजीव गांधी होते तो कांग्रेस वैसी नहीं होती, जैसी हो गई है। और, कांग्रेस ऐसी न हो गई होती तो नरेंद्र भाई सात जनम भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे।
यह तो भला हो सोनिया गांधी का कि उन्होंने सीताराम केसरी के समय अंधे कुएं में डूब रही कांग्रेस को खींच कर बाहर निकाल लिया और दो दशक से ज़्यादा हो गए हैं कि उसकी देखभाल में अपने दिन-रात एक कर रही हैं। दो साल से अपने क्षोभ-भवन में बैठे राहुल गांधी की तकनीकी अनुपस्थिति में भी सोनिया की वज़ह से ही कांग्रेस संतुलन-बांस के सहारे सियासत की रस्सी पर एक-एक कदम आगे बढ़ा पा रही है। सोचिए कि अगर तमाम दबावों, मजबूरियों और घुसपैठियों की कुचालों का बावजूद सोनिया की विवेकवान अगुआई कांग्रेस के भाग्य में न होती तो उसके कितने परखच्चे बिखर चुके होते? विपक्षी-दादुरों के लिए एक मर्तबान में ठोस ज़गह बनाने के लिए भी उन्होंने इसीलिए राजीव गांधी के जन्म का दिन चुना कि अपनी अलविदाई के तीन दशक बाद भी राजीव भलमनसाहत और वचनबद्धता के सबसे बड़े प्रतीक हैं।
दो साल पहले राहुल गांधी ने जब कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ा, तब भी उनका फ़ैसला मेरी समझ से बाहर था। अब दो बरस से उन्हें सारी मान-मनुहार की अनदेखी करते देख तो मैं ने अपनी अक़ल को घास चरने के लिए छोड़ दिया है। कौन-सा ऐसा राजनीतिक दल दुनिया में होगा, जिसके सदस्य किसी की दहलीज़ पर इतनी बार अपने सिर पटक-पटक कर रोते होंगे? और, किस राजनीतिक दल में ऐसा कोई होगा कि आंसुओं की इतनी निष्ठुर अनदेखी करता होगा? राहुल के अगलिए-बगलिए अगर उन्हें यह समझा रहे हैं कि इन सब को अभी और रोने दो तो कोई उन्हें समझाए कि एक दिन आता है कि आंसू भी सूख जाते हैं। वह दिन भी आता है कि आंसू अंगारे बन जाते हैं। ईश्वर करे कि वह दिन न आए। आया तो सबसे पहले, सूरजमुखी के जिन फूलों की बेतरतीब फ़सल छह साल से लहलहा रही है, वह भस्म होगी। गिरिधर-मुद्रा में पसर कर मोहिनीयट्टम कर रहे चिरकुटों की बांसुरियां स्वाहा होंगी।
मैं तो अपने पिता के जन्म दिन पर अगले साल के लिए संकल्प धारण करता हूं। मैं राजीव गांधी के जन्म दिन पर भी एक संकल्प लेता हूं। मुझे नहीं मालूम कि राहुल गांधी ने अपने पिता के जन्म दिन पर इस बार क्या संकल्प लिया है। मुझसे पूछते तो मैं उनसे कहता कि आप पर अपने पिता का जो कर्ज़ है, ‘ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः’ बोल कर इस साल उससे मुक्ति का संकल्प लीजिए। भेड़ियों, सियारों, लोमड़ियों और गिरगिटों को परे ठेलिए। राजसूय यज्ञ की तैयारियां कीजिए। यह अश्वमेध यज्ञ का नहीं, राजसूय यज्ञ का समय है। यह बहेलियों के जाल को तार-तार करने का वक़्त है। ‘नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने । विक्रमार्जितसत्त्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता ।।’ शेर को जंगल का राजा नियुक्त करने के लिए न तो कोई राज्याभिषेक किया जाता है और न कोई पूजा-पाठी संस्कार। राहुल मुझ नाचीज़ की सुनें तो ठीक, न सुनें तो ठीक। अपनी बात कहना अपना काम है।(लेखक न्यूज़-व्यूज़ इंडिया के संपादक और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं।)